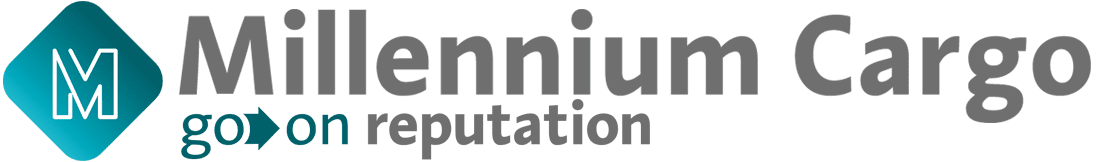कुछ सप्ताह पहले मैं एस्टन विला का खेल देखने के लिए एम्स्टर्डम गया था।
यह यात्रा भी किसी भी अन्य यात्रा की तरह ही शुरू हुई... जल्दी निकले, ल्यूटन पहुँचे, गाड़ी पार्क की, कोई तामझाम नहीं हुआ। हवाई अड्डे जाने वाली ट्रेन समय पर थी। उड़ान थोड़ी देर से हुई, लेकिन ईज़ीजेट ने ठीक काम किया - हमें सूचित रखा और कुछ ही देर में हम हवा में थे। हम उतरे, सीधे शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए, होटल में चेक-इन किया, और कुछ अच्छा खाना और एक-दो पिंट पीने निकल पड़े। सब कुछ बस... काम कर गया। जैसा होना चाहिए... अगले दिन, मैं रॉटरडैम के लिए रवाना हो गया। हम वहाँ काफ़ी समय से पहुँच गए, रिस्टबैंड लिए और माहौल का आनंद लिया। फिर हम "आखिरी मील" पर पहुँचे।
हम लगभग 7:15 बजे स्टेडियम स्टेशन पहुँचे। किक-ऑफ़ 9 बजे से पहले नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अंदर चलते हैं, कुछ पीते हैं, शायद अपनी सीटें पहले ही ढूँढ़ लेते हैं और सब कुछ देखते हैं। असल में क्या हुआ? एकदम अफ़रा-तफ़री। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, ऐसा लगा जैसे हम असमंजस में फँस गए हों। कुछ समझ ही नहीं आया, हमें मैदान के ठीक बाहर एक बाड़े से घिरे हुए होल्डिंग एरिया में ठूँस दिया गया। हममें से हज़ारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर, मवेशियों की तरह ठूँसे हुए थे। न शौचालय। न पानी। न छाया। और सबसे बुरी बात - कोई जानकारी नहीं। वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था जो बता सके कि क्या हो रहा है या हमें स्टेडियम में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और जितनी देर हम वहाँ खड़े रहे, उतना ही ज़्यादा निराशा होती गई - सिर्फ़ इंतज़ार की वजह से नहीं, बल्कि सन्नाटे की वजह से भी।
स्टेडियम सचमुच कुछ सौ मीटर की दूरी पर था। हम उसे देख सकते थे। तैयारियों की आवाज़ सुन सकते थे। खाने-पीने के स्टॉल की खुशबू महसूस कर सकते थे। लेकिन हम हिल नहीं पा रहे थे। जब किक-ऑफ हुआ, तब तक हम अभी भी बाहर फंसे हुए थे - गर्मी, निराशा और पूरी तरह से अंधेरे में। लोग उत्तेजित हो रहे थे। छोटे बच्चों वाले परिवार थे, लाठी लिए बुज़ुर्ग प्रशंसक थे - किसी को नहीं पता था कि हमें क्यों रोका जा रहा है, कितनी देर के लिए, या हम अंदर जा भी पाएँगे या नहीं। और सच कहूँ तो - अगर मुझे पता होता कि मुझे लगभग तीन घंटे तक एक बाड़े में खड़ा रहना पड़ेगा, इस तरह ठसाठस भरा हुआ, अपने कम उम्र के घुटनों के बल खड़ा रहना पड़ेगा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है... तो शायद मैं वहाँ जाता ही नहीं।
और सबसे अजीब बात? बाकी सब तो बहुत बढ़िया चल रहा था। फ्लाइट, ट्रेन, होटल, रिस्टबैंड – सब कुछ ठीक-ठाक। बस एक चीज़ जो बिखर गई? आखिरी 500 मीटर। वो आखिरी मील।
और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम माल ढुलाई के मामले में क्या करते हैं। हम आँखें बंद करके चीन से ब्रिटेन तक सामान पहुँचा सकते हैं। महासागर पार कर सकते हैं, सही बंदरगाह पर उतर सकते हैं, कस्टम्स क्लियर कर सकते हैं... लेकिन अगर आखिरी पड़ाव - गोदाम से ग्राहक के दरवाज़े तक सामान पहुँचाना - गड़बड़ा जाए, तो यही बात उन्हें याद रहती है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि कितने कंटेनर समय पर पहुँचे। उन्हें इस बात की परवाह है कि उनका सामान देर से पहुँचा। या पहुँचा ही नहीं। या इससे भी बदतर - कि किसी ने फ़ोन उठाकर उन्हें यह नहीं बताया कि क्या हो रहा है।
क्योंकि बात ये है... लोग समस्याओं के साथ जी सकते हैं। देरी होती है। सड़कें बंद हो जाती हैं। सामान अटक जाता है। ये आदर्श तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी यही है। जिस चीज़ के साथ वे जी नहीं सकते, वो है खामोशी। कुछ पता न होना। अँधेरे में छोड़ दिए जाना। यही एक छोटी सी देरी को भी एक वाजिब शिकायत में बदल देता है। इसलिए अगर आप इस खेल में हैं - चाहे वो माल ढुलाई हो, ग्राहक सेवा हो, डिलीवरी हो, कुछ भी हो - तो आखिरी पड़ाव पर हार मत मानिए।
और अगर चीज़ें भी जाएँ, तो यूँ ही चुप मत रहो और उम्मीद मत करो कि सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन उठाओ। ईमेल भेजो। कुछ कहो। लोग सफ़र की शुरुआत से ज़्यादा उसके अंत को याद रखते हैं – इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम मज़बूती से अंत करो। या कम से कम, उन्हें स्टेडियम के बाहर फँसा मत छोड़ो, यह सोचते हुए कि आख़िर हो क्या रहा है।